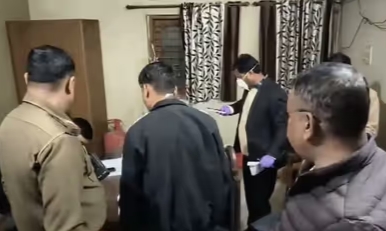Holi : हिन्दी ललित निबंध परम्परा के महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर, सांस्कृतिक निबंधकार एवं भारतीय आर्ष चिंतन के गन्धमादन कुबेरनाथ राय कहते हैं कि ‘भारत’ के तीन रूप हैं : मृण्मय भारत, शाश्वत भारत और चिन्मय भारत। भारत का मृमन्य रूप हमारे नदी, पहाड़, वन, गाँव-नगर, खेत-खलिहान और हाट-बाजार में उपस्थित है। भारत का शाश्वत रूप सैन्धव सभ्यता के पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक भारत के अविच्छिन्न, सतत प्रवहमान इतिहास है। मैं समझता हूँ कि भारत का चिन्मय रूप हमारे प्राचीन वाङ्गमय, साधना, शिल्प, साहित्य, दार्शनिक चिन्ता के अलावा हमारे देश की उत्सवधर्मिता अर्थात् देश के पर्व, त्यौहार और उत्सवों में भी व्यक्त होता है। इन त्यौहारों में देश भर में अलग-अलग नामों से जैसे, असम में ‘डोलजात्रा और देउल’, बंगाल और ओडिशा में ‘डोलजात्रा’, महाराष्ट्र में ‘रंग पंचमी’, गुजरात में ‘राजा की होली’ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में ‘होरी’, उत्तर प्रदेश और बिहार में होली और ‘फगुआ’, हरियाणा में ‘धुलेंडी’, पंजाब में ‘होला मोहल्ला’, कुमाऊँ में ‘गीत बैठकी’, मणिपुर में ‘ याओसांग’, गोवा में ‘शिमगो’, आंध्र प्रदेश में ‘कामुनी पंडुगा’, तमिलनाडु में ‘कमान पंडिगईं’, कर्नाटक में ‘कामना हब्बा’ और अलग-अलग रूपों में मनाया जाने वाला होली का त्योहार है। होली का एक नाम रंगोत्सव है। रंगोत्सव बड़ा ही सार्थक नाम है। मनुष्य का रंगों से रागात्मक संबंध रहा है। रंग न हों तो जीवन बेरंग हो जाय,मनुष्य की जिजीविषा असमय मुरझा जाय। इस सृष्टि में न जाने कितने रंग बिखरे हैं। एक कवित्त में इन रंगों का वर्णन है-
धानी,आसमानी, सुलैमानी, मुलतानी, मूंगी
संदली, सिंदूरी, सुख; सोसनी सुहाये हैं
कंजई, कनेरी, भूरे; चम्पई, जंजीरी हरे
पिस्तई, मजीठी, सुरमई घेरे आये हैं
भासी, नीलकंठी, गुलबासी, सुखरासी, तुसी
कुसुमी, कपासी, रंग पूरब दिखाये हैं
नारंगी, पियाजी, पोखराजी, गुलनारी घन
केसरी, गुलाबी, सुआपँखी मेघ छाये हैं
हमारे सारे त्योहार किसी न किसी ऋतु से जुड़े हैं। होली वसन्त ऋतु का त्योहार है। प्रति वर्ष माघ शुक्ल पंचमी को धरती पर वसन्त के आगमन की सूचना फैल जाती है। उसी दिन होली का ताल भी ठोका जाता है। वसन्त की शोभा, उसका फुल्ल-कुसमित रूप, गन्ध, गान आत्मा में अतीव उल्लास भर देता है। मन में जड़ीभूत हिमराशि पिघलने लगती है, धरती के सीने से चिपकी मृत घास अचानक जी उठती है, मन और देह में गरम पानी के सोते फुट पड़ते हैं और लगता है धरती पर अदृश्य गन्धमादन पर्वत उतर आया है। वसन्त वानस्पतिक चेतना की ऋतु है, सृष्टि व्यापी काम भाव के उन्मेष की ऋतु है। यह अकारण नहीं कि कृष्ण ने गीता में कहा-ऋतुनां अहं कुसुमाकर: अर्थात् ऋतुओं में में वसन्त ऋतु हूँ। गुप्तकाल में मनाया जाने वाला वसन्तोत्सव और मदनोत्सव कालांतर में होली के रूप में प्रचलित हुआ।
होली के परम्पराएँ अत्यंत प्राचीन हैं। आर्यों में होली पर्व का प्रचलन था। वैदिक काल में इसे ‘नवत्रैष्टि यज्ञ’ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपक्के अन्न यज्ञ में दान करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का विधान था। कच्चे अन्न को ‘होला’ कहते हैं। इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। जैमिनी के मीमांसा सूत्र, पारस्कर के गृह्यसूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण में इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ में ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में होली पर्व का उल्लेख है। मौर्यकालीन भारत में वसन्तोत्सव के रूप में होली पर्व मनाया जाता था। हर्ष की ‘प्रियदर्शिनी’ और ‘रत्नावली’, कालिदास के ‘कुमारसंभवम्’, ‘मालविकाग्निमित्रम्’ और ऋतुसंहार’ में होली त्यौहार का उल्लेख है।
प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अलबेरुनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा-संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होली का उत्सव केवल हिन्दू ही नहीं मुसलमान भी मनाते थे। अकबर का जोधाबाई के साथ होली खेलने का उल्लेख है। अलवर के संग्रहालय में 400 वर्ष पुराने एक मुगलकालीन चित्र में जहाँगीर को नूरजहाँ एवं अन्य स्त्रियों के साथ होली खेलते हुए दिखाया गया है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को होली के अवसर पर उनके मंत्रिगण रंग लगाया करते थे।
होली कवियों का प्रिय विषय रहा है। हिन्दी के प्रथम कवि ने अपने महाकाव्य ‘पृथ्वीराज रासो’ में होली का वर्णन किया है। विद्यापति से लेकर भक्तिकाल के कवि कबीर,जायसी, सूर, रहीम, रसखान और मीराबाई; रीतिकाल के बिहारी, केशव, पद्माकर और घनानंद; भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी ‘प्रेमघन’; छायावादी कवियों में पन्त, जयशंकर प्रसाद और निराला, छायावोदोत्तर काल के मैथिलीशरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंशराय ‘बच्चन’, रामधारी सिंह ‘दिनकर’, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, गोपाल प्रसाद ‘नीरज’, केदारनाथ सिंह, एकांत श्रीवास्तव और नवगीत के गीतकारों ने होली पर कविताएँ और गीत लिखे हैं। मुस्लिम कवियों में सूफी कवि हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, नजीर बनारसी ने होली पर गीत और गजल लिखे हैं।
होली रंगों का इंद्रधनुषी उत्सव है, मुख्य घटक हैं रंग, गीत, संगीत और मस्ती। होली में बरसते रंग, उड़ते गुलाल, वसन्त का प्रांजल, प्रेमिल संस्पर्श और गीत-संगीत का निर्झर मन में उल्लास और उमंग भर देते हैं और मनमृग चौकड़ी भरने लगता है। शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन तथा लोकगीत दोनों में होली का विशेष स्थान रहा है। शास्त्रीय गायन की ध्रुपद और धमार शैली, उपशास्त्रीय गायन की ठुमरी, दादरा और टप्पा शैली में बहुत ही सुंदर होली गीत गाये गए हैं। ठुमरी शैली में शोभा गुर्टू द्वारा गाया गया होली गीत ‘आज बिरज में होली रे रसिया’ और गिरिजा देवी द्वारा ‘तुम करत बरजोरी’ आज में मन को सराबोर कर देते हैं।
भोजपुरी होली गीत, ‘राम खेले होरी, लछुमन खेले होरी/ गढ़ लंका में रावण खेले होरी, ‘लड़िका हो गोपाल, लड़िका हो गोपाल/ कूदी पड़े जमुना में कन्हैया, हनुमान लला हो/ हम तोहरे बलिहारी; मगही होली गीत,’ खेलत बीर हनुमान/राम के चरनिया में होरी; मैथिली होली गीत, ‘जमुना तट स्याम खेलत होरी/कसि कसि स्याम भरत पिचकारी/राधा कृष्ण खेलत होरी; बज्जिका होली गीत,’फागुन में राम खेलत होरी, फागुन में/रामजी का हाथ कनक पिचकारी/हो हो सीताजी के हाथ अबीर की झोरी; अंगिका होली गीत, ‘शिव मठ पर आज मच्यो होरी, शिव मठ पर/ भोरे-भोरे गणपति खेलयs कार्तिक खेलयs दुपहरिया हो’ के अलावा अवधी होली गीत, ‘अवध मां होली खेलत रघुबीरा/रामजी के हाथ ढोल झाल सोहे/लछुमन के हाथ मजीरा’ खूब प्रचलित है। ब्रजभाषा का होली गीत, “आज बिरज में होली रे रसिया’ की धूम तो है ही।
हँसी-ठठोली, सौहार्द्र, सामाजिक समरसता और समन्वय का संदेश हर लोकगीत में है। ‘भर फागुन बुढ़ऊ देवर लगिहैं’, ‘एक ओर खेलत कृष्ण कन्हैया/एक ओर राधा होरी हो’ और ‘सदा आनन्द रहे एहि द्वारे’ हर भाषा के लोकगीत में है।
होली अकेला ऐसा त्यौहार है जो समतामूलक समाज की परिकल्पना को साकार करता है। इस त्यौहार में जाति-धर्म, अमीरी-गरीबी, ऊँच-नीच के सारे भेदभाव मिट जाते हैं। होली का रसबोध हमारे यांत्रिक जीवन में सुकून दे जाता है। होली एक परम्परा का नाम है, एक लोक ससंस्कृति है जो हमारे कानों में फुसफुसा कर कहती है-‘एकरंगा जीवन उबाऊ होता है,भीतर का उत्सव-भाव मरना नहीं चाहिए, जीवन के रंग फीके नहीं पड़ने चाहिए।’ मन से ज्यादा उपजाऊ जमीन कहीं नहीं है। इसमें जो कुछ बोया जाय तेजी से फैलता है, चाहे प्यार हो या नफरत। तो आइए होली के इस अवसर पर मन की जमीन में प्यार का बीज बोने का संकल्प लें।
Holi : रंगों का इंद्रधनुषी उत्सव है होली

Leave a Comment
Leave a Comment